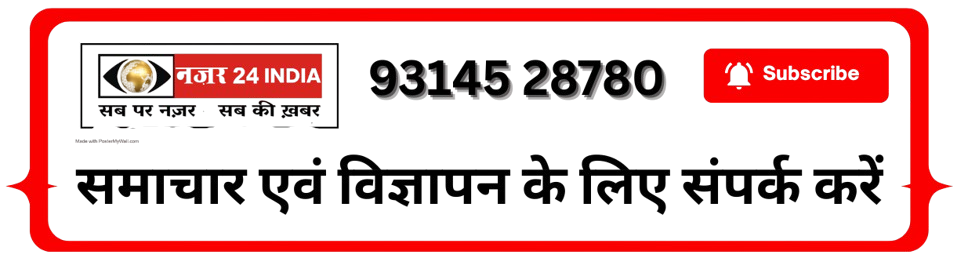बदलते संस्कारों पर एक दृष्टि — सुनिता त्रिपाठी’अजय’

भारतीय समाज अपनी पहचान सदियों से संस्कारों, मर्यादा और जीवन-मूल्यों से पाता रहा है। यहाँ अनुष्ठानों की गरिमा केवल रीति नहीं, बल्कि मनुष्य के चरित्र को दिशा देने वाली परंपरा रही है। लेकिन बदलते समय और बढ़ते बाज़ार के बीच यह चिंता लगातार गहराती जा रही है कि क्या आधुनिकता के नाम पर हम उन संवेदनाओं से दूर होते जा रहे हैं जो हमारी संस्कृति की आत्मा थीं?
पिछले कुछ वर्षों में विवाह और उत्सवों की परंपराएँ एक नए रूप में उभरी हैं। आज साड़ी पहनाने के लिए प्रोफेशनल पुरुष ड्रेपर्स बुलाए जा रहे हैं, मेहंदी और टैटू आर्ट में पुरुष बड़ी संख्या में आ रहे हैं, दुल्हन की ड्रेस-फिटिंग और मेकअप तक में पुरुषों की मौजूदगी आम हो गई है। यह बदलाव सुविधा और व्यवसाय का परिणाम है, पर इसके साथ कई सांस्कृतिक प्रश्न खड़े होते हैं—जो केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक संदर्भों से भी जुड़े हैं।
हमारी परंपरा में स्त्री की निजता और मर्यादा को अत्यंत स्नेह और सम्मान से संरक्षित किया गया। धार्मिक अनुष्ठानों में भी स्पर्श को लेकर इतनी सूक्ष्म मर्यादा थी कि पुजारी तक महिलाओं को तिलक लगाने से बचते थे। यह केवल नियम नहीं, बल्कि स्त्री-गरिमा की गहरी समझ थी।
ऐसे में यह विचार स्वाभाविक है कि जो कार्य परंपरागत रूप से स्त्री के निजी दायरे में थे—जैसे वस्त्र-सज्जा, श्रृंगार, साड़ी पहना देना—वे आज खुले व्यावसायिक क्षेत्र में पुरुषों द्वारा तेजी से किये जा रहे हैं। यह परिवर्तन सुविधा का प्रतीक है या मर्यादा के क्षरण का? यह प्रश्न समाज को कहीं भीतर तक सोचने पर विवश करता है।
इसी संदर्भ में महाभारत की द्रौपदी का प्रसंग भारत की सांस्कृतिक चेतना में बार-बार याद आता है। उस युग में एक स्त्री की साड़ी खींचने का प्रयास इतना बड़ा अपमान माना गया कि उससे एक महायुद्ध की भूमिका बन गई। वहाँ नारी-गरिमा की रक्षा धर्म का पहला कर्तव्य थी।
आज स्थिति अलग है—पर प्रतीक वही हैं। द्रौपदी का प्रसंग हमें यह स्मरण कराता है कि भारतीय समाज में स्त्री की निजता केवल व्यक्तिगत मुद्दा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना का मूल है। और जब आज स्त्रियाँ स्वयं ही कई बार सुविधा या ट्रेंड के नाम पर वही सीमाएँ सहजता से छोड़ रही हैं, तो यह स्थिति समाज के भीतर एक गहरे परिवर्तन की ओर संकेत करती है।
आधुनिकता आवश्यक है, प्रगति भी अनिवार्य है, पर प्रगति तब ही सुंदर होती है जब वह मर्यादा के प्रकाश में चलती है।
यह विचार किसी बंदिश का नहीं, बल्कि संतुलन का है। यह कहना नहीं कि पुरुष इन क्षेत्रों में न आएँ, बल्कि यह समझना कि कौन-सा कार्य सुविधा है और कौन-सा व्यक्तिगत सीमा में अतिक्रमण।
समाज को वह रूप चाहिए जिसमें सुविधा भी हो, संवेदना भी; आधुनिकता भी हो, मर्यादा भी; विकल्प भी हों, पर सांस्कृतिक चेतना भी जीवित रहे।
द्रौपदी के प्रसंग की स्मृति हमें यह बताती है कि स्त्री-गरिमा का अपमान कभी भी समाज के लिए शुभ नहीं रहा—और उसकी रक्षा केवल समाज की नहीं, स्त्रियों की भी साझा जिम्मेदारी है।
आज समय फिर उसी प्रश्न पर खड़ा है—
क्या हम आधुनिकता और परंपरा के बीच ऐसा पुल बना पाएँगे जो सुविधा को भी स्वीकार करे और संस्कृति की आत्मा को भी सुरक्षित रखे?
सुनिता त्रिपाठी’अजय’
जयपुर राजस्थान