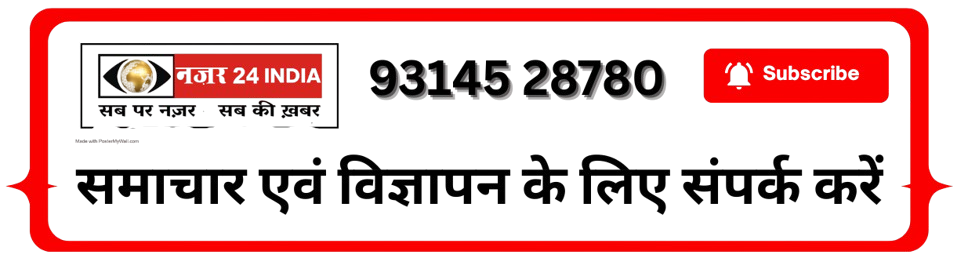संविधान: अधिकारों की आजादी या प्रतिबंधों की जकड़न? — मंजू शर्मा ‘मनस्विनी’

26 नवम्बर का दिन हमारे लोकतंत्र के इतिहास में खास है। इसी दिन 1949 में भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। किताबों में हमने पढ़ा कि यह संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है—बोलने की स्वतंत्रता, जीने का अधिकार, धर्म मानने की आज़ादी, समानता का अधिकार और भी बहुत कुछ। लेकिन जैसे-जैसे ज़िन्दगी को समझा तो समाज में अनुभव पाए, अक्सर महसूस हुआ कि किताबों और असल ज़िन्दगी में फर्क है।
हम सभी को बचपन से सिखाया जाता है। “भारत एक स्वतंत्र देश है, यहां हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है।” पर जैसे ही हम किसी संवेदनशील विषय पर, खासकर धर्म या राजनीति पर बोलते हैं, तुरंत कहा जाता है—”चुप रहो, यह मत कहो।” मुझे कई बार लगा कि बोलने की स्वतंत्रता तो है, पर उसके साथ इतनी शर्तें और रोक-टोक जुड़ी हैं कि असली स्वतंत्रता का अर्थ खो जाता है।
संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। लेकिन उसी के साथ अनुच्छेद 19(2) में इतनी लंबी “रेस्टिक्शन” की सूची जोड़ दी गई है। राज्य की सुरक्षा, नैतिकता, सदाचार, शांति, भाईचारा, न्यायपालिका की गरिमा आदि। नतीजा यह होता है कि आप कह सकते हैं, लेकिन हमेशा डर के साथ। यानी अधिकार दिए गए, पर जीने की जगह प्रतिबंधों की जंजीरें भी साथ बांध दी गईं।
यह बात मुझे मेरी अपनी जिन्दगी के कई छोटे-छोटे अनुभवों से समझ आई। एक बार किसी ने बताया कि मैंने एक सभा में धर्म के नाम पर फैले दिखावे पर सवाल उठाया था। उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुँचाना नहीं था, बस समाज की समस्याओं की ओर ध्यान खींचना था। लेकिन तुरंत माहौल बदल गया-लोग कहने लगे कि “धर्म के बारे में मत बोलो, यह विवाद का कारण बन सकता है।”उस दिन महसूस हुआ कि संविधान कहता है, “धर्म मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है पर व्यवहार में वह स्वतंत्रता आधी-अधूरी ही है।
कुछ ऐसा ही हाल विचारों का भी है। आप राजनीतिक नेताओं पर टिप्पणी करें, तो समर्थक नाराज हो जाते हैं। आप किसी सामाजिक कुरीति पर बोलें, तो लोग कहते हैं “समाज बिगड़ जाएगा।” इस तरह से तो स्वतंत्रता एक दिखावा मात्र लगती है—जैसे घर में माता-पिता कहते हैं बच्चों को, तुम्हें अपनी पसंद का खाना खाने की आज़ादी है, पर यह मत खाना, वह मत खाना।” आखिर यह कैसी आज़ादी हुई, जिसमें हर कदम पर रेस्टेक्शन ही लिखा हो?
संविधान दिवस पर जब हम इस महान ग्रंथ को याद करते हैं, तब हमें उसकी आत्मा को समझना चाहिए। संविधान केवल किताबों की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं बना। यह नागरिकों को ताकत देने के लिए बना है। लेकिन आज नागरिक अक्सर डर में जीते हैं। डर इस बात का कि अगर उन्होंने सच कहा, तो उन पर मुकदमा हो जाएगा, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो जाएगी, या समाज उन्हें अलग-थलग कर देगा।
संविधान दिवस हमें यही सोचने का अवसर देता है-क्या हम केवल अधिकारों की सूची से संतुष्ट हैं? या हमें उस स्तर तक पहुंचना चाहिए, जहां हर नागरिक बिना डर, बिना दिखावे और बिना शर्त अपनी बात कह सके।
आज के समय में हमें यह स्वीकार करना होगा कि अधिकारों का अर्थ केवल ‘पाने’ में नहीं, बल्कि ‘जीने’ में है। अगर हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो हमें उसे इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि न तो दूसरों की आस्था को चोट पहुंचे और न ही सच दबे।
संविधान हमें यह भी सिखाता है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ चलते हैं। केवल अधिकार मांगना ही काफी नहीं है, हमें यह भी देखना होगा कि हमारे शब्द समाज में भाईचारे और एकता को तोड़ते नहीं हो।
आज जरूरत इस बात की है कि संविधान को एक “जीवंत दस्तावेज़” की तरह जिया जाए। यह केवल अदालतों और संसद की चीज़ नहीं है, यह हमारे रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा है। जब हम घर में, दफ़्तर में, समाज में बिना भय के अपनी बात रख पाएंगे, तभी हम कह सकेंगे कि हमने सच में संविधान को अपनाया है।
हमें बोलने की आज़ादी का इस्तेमाल ज़िम्मेदारी से करना चाहिए—ऐसा कि किसी की आस्था को ठेस न पहुँचे, लेकिन साथ ही सच्चाई भी दबाई न जाए। यही संविधान की आत्मा है—अधिकार और कर्तव्य का संतुलन।
संविधान दिवस पर मैं यही संदेश देना चाहूंगी—
अधिकार हमें किताबों में पूरे मिले हैं,
पर जीवन में आधे ही जी पाए हैं।
अधिकारों के साथ जुड़े हैं कर्तव्य
जो हमने कम ही निभाये हैं
अब समय है कि हम उन अधिकारों को पूरी तरह जीना सीखें,और संविधान की आत्मा को व्यवहार में लाएं।
मंजू शर्मा ‘मनस्विनी’
कार्यकारी संपादक